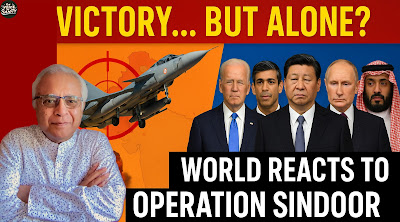23 मई से भारत दुनिया भर के प्रमुख देशों में राजनेताओं की आठ टीमें भेज रहा है। प्रत्येक टीम में विभिन्न राजनीतिक दलों के कम से कम पाँच सांसद हैं। वरिष्ठ राजनयिक और विशेषज्ञ उनके साथ शामिल होंगे। यह प्रयास ऑपरेशन सिंदूर के बाद किया गया है। इसका प्रत्यक्ष लक्ष्य आतंकवाद के खिलाफ भारत के एकजुट रुख को दिखाना और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करना है। यह ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने में भारत के सशस्त्र बलों की असाधारण उपलब्धि से मेल खाने में भारत की कूटनीति की विफलता का भी संकेत है।
यह पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाने वाला एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध सैन्य अभियान था। इसे "सटीक और गैर-बढ़ाने वाला" हमला बताया गया, इस अभियान का उद्देश्य जैश-ए-मोहम्मद (JeM), लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे समूहों से जुड़े आतंकी शिविरों को बेअसर करना था। यह ऑपरेशन एक सैन्य सफलता थी। इसने भारत की उन्नत गैर-संपर्क युद्ध क्षमताओं को प्रदर्शित किया। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया ने इसकी विदेश नीति में खामियों को उजागर किया। इसके किसी भी पड़ोसी ने ऑपरेशन सिंदूर का मुखर समर्थन नहीं किया। यूरोपीय संघ, क्वाड सदस्य, अमेरिका, ब्रिटेन, अरब देश और यहां तक कि रूस जैसे पारंपरिक सहयोगी जैसे प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी या तो पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए या तटस्थ रहे। तो, क्या भारत की सैन्य सफलता ने उसके मित्रों को अलग-थलग कर दिया है? उनके तटस्थ या पाकिस्तान समर्थक रुख के पीछे क्या कारण हैं? और, भारत की विदेश नीति के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं?
ऑपरेशन सिंदूर पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ
ऑपरेशन सिंदूर पर यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया आतंकवाद की निंदा और तनाव कम करने के आग्रह के बीच एक नाजुक संतुलन को दर्शाती है। यूरोपीय संघ और उसके 27 सदस्य देशों ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि "हर राज्य का कर्तव्य और कानूनी रूप से अपने नागरिकों को आतंकवादी कृत्यों से बचाने का अधिकार है।" हालांकि, इसने बढ़ते तनाव पर "बड़ी चिंता" भी व्यक्त की और भारत और पाकिस्तान दोनों से "संयम बरतने, तनाव कम करने और नागरिकों की जान बचाने के लिए आगे के हमलों से बचने" का आह्वान किया। यह स्थिति, भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार करते हुए, उसके सैन्य प्रतिक्रिया के पैमाने की परोक्ष रूप से आलोचना करती है। यूरोपीय संघ का सतर्क रुख संभवतः दक्षिण एशिया में स्थिरता की उसकी इच्छा से उपजा है, जो वैश्विक व्यापार और ऊर्जा मार्गों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत-पाकिस्तान जैसे परमाणु फ्लैशपॉइंट में युद्ध की बजाय संवाद के लिए इसकी प्राथमिकता काफी स्पष्ट है।
क्वाड (जिसमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं) ने अपनी प्रतिक्रिया में संयम बरता है। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हयाशी ने "गहरी चिंता" व्यक्त की कि ऑपरेशन सिंदूर एक "पूर्ण पैमाने पर सैन्य संघर्ष" में बढ़ सकता है। उन्होंने दोनों देशों से बातचीत के जरिए स्थिति को स्थिर करने का आग्रह किया। ऑस्ट्रेलिया काफी हद तक चुप रहा है। क्वाड का प्राथमिक ध्यान इंडो-पैसिफिक में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने पर है क्वाड भागीदारों से मुखर समर्थन की कमी से पता चलता है कि भारत की सैन्य कार्रवाइयाँ, सामरिक रूप से सफल होने के बावजूद, क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और भारत-पाकिस्तान तनाव में उलझने से बचने के गठबंधन के व्यापक उद्देश्यों के साथ संरेखित नहीं हो सकती हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरा दृष्टिकोण अपनाया है। इसने संयम बरतने का आग्रह करते हुए आतंकवाद से लड़ने के भारत के अधिकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मॉर्गन ब्रूस ने बातचीत की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत की सक्रिय कूटनीति, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष को जानकारी दी, ने सुनिश्चित किया कि वाशिंगटन को ऑपरेशन के गैर-बढ़ावा देने वाले इरादे के बारे में सूचित किया जाए। हालाँकि, अमेरिका का सतर्क रुख पाकिस्तान में उसके रणनीतिक हितों को दर्शाता है, जिसमें अफ़गानिस्तान को स्थिर करने में उसकी भूमिका भी शामिल है। जाहिर है, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत की कार्रवाइयों के लिए सीधे समर्थन के बजाय तनाव कम करना पसंद करता है।
ब्रिटेन की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही है। पूर्व प्रधान मंत्री ऋषि सुनक ने कहा, "किसी भी देश को दूसरे देश द्वारा नियंत्रित भूमि से उसके खिलाफ किए जा रहे आतंकवादी हमलों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। भारत द्वारा आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर हमला करना उचित है।" इसी तरह, छाया विदेश सचिव प्रीति पटेल ने आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए भारत के “उचित कदमों” का समर्थन किया। हालांकि, विदेश मंत्री डेविड लैमी द्वारा व्यक्त की गई आधिकारिक यूके स्थिति ने दोनों देशों से “संयम दिखाने और बातचीत में शामिल होने” का आग्रह किया।
अरब देशों, खास तौर पर यूएई, सऊदी अरब और कतर ने पक्ष लेने के बजाय मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद ने संकटों को हल करने के साधन के रूप में कूटनीति और संवाद का आह्वान किया। कतर के विदेश मंत्रालय ने "गहरी चिंता" व्यक्त की और अच्छे पड़ोसी और कूटनीतिक समाधानों की बात की। सऊदी अरब के विदेश मामलों के राज्य मंत्री, अदेल अल-जुबेर ने तनाव को शांत करने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया। ये प्रतिक्रियाएँ भारत और पाकिस्तान दोनों में खाड़ी देशों के आर्थिक और रणनीतिक हितों से प्रेरित हैं। उदाहरण के लिए, यूएई और सऊदी अरब के भारत के साथ महत्वपूर्ण व्यापार और निवेश संबंध हैं। खाड़ी में पाकिस्तान के बड़े प्रवासी कार्यबल और क्षेत्रीय सुरक्षा में इसकी भूमिका, विशेष रूप से ईरान के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए, तटस्थता को एक व्यावहारिक विकल्प बनाती है।
बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान सहित भारत के पड़ोसी देश या तो चुप रहे हैं या ऑपरेशन सिंदूर का पूरी तरह से समर्थन किए बिना भारत का सावधानीपूर्वक समर्थन किया है। बांग्लादेश ने सीमा पार उग्रवाद पर चिंता व्यक्त की, लेकिन हमलों का समर्थन करने से परहेज किया। नेपाल के मुख्यमंत्रियों ने ऑपरेशन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी, लेकिन यह सीमावर्ती राज्यों तक ही सीमित था और राष्ट्रीय रुख नहीं था। भारत के सैन्य दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाने में क्षेत्रीय हिचकिचाहट प्रतीत होती है। यह अनिच्छा भारत-पाकिस्तान संघर्ष में घसीटे जाने के डर से उत्पन्न हो सकती है। घरेलू राजनीतिक दबाव हो सकते हैं, जैसा कि बांग्लादेश के संतुलनकारी कार्य में देखा गया है।
पाकिस्तान का कथन, जिसे उसके सैन्य और विदेश मंत्रालय द्वारा बढ़ाया गया है, भारत के हमलों को संप्रभुता के "अकारण उल्लंघन" के रूप में चित्रित करता है। इसने नागरिक हताहतों और मस्जिदों जैसे गैर-सैन्य लक्ष्यों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया। भारतीय सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों सहित पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई को रक्षात्मक प्रतिक्रिया के रूप में तैयार किया गया था। तुर्की ने पाकिस्तान का पुरजोर समर्थन किया है। इसने भारत की कार्रवाइयों को "पूरी तरह से युद्ध" का जोखिम बताया है। पाकिस्तान के लिए वैश्विक सहानुभूति, विशेष रूप से इस्लामी देशों से, आंशिक रूप से नागरिक नुकसान और मुजफ्फराबाद में बिलाल मस्जिद जैसी जगहों को निशाना बनाने के उसके दावों के कारण है। यह कथन भारत के सटीक हमलों के दावे को चुनौती देता है और तनाव कम करने की मांग को हवा देता है।
तटस्थ या पाकिस्तान समर्थक रुख क्यों?
भारत-पाकिस्तान संघर्ष दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु फ्लैशपॉइंट में से एक है। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और जापान जैसे क्वाड सदस्यों ने व्यापक संघर्ष में वृद्धि को रोकने के लिए संयम पर जोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का यह कथन कि "दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव बर्दाश्त नहीं कर सकती" इस डर को रेखांकित करता है।
भारत के एकतरफा हमलों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा के रूप में उचित ठहराया गया है। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की संप्रभुता के उल्लंघन के बारे में भी चिंता जताई। चीन और तुर्की ने भारत की कार्रवाई की आलोचना की है। चीन ने दोनों पक्षों से "ऐसी कार्रवाइयों से परहेज करने का आह्वान किया जो स्थिति को और जटिल बना सकती हैं।" अमेरिका, अरब देशों और यहां तक कि रूस के भी पाकिस्तान में रणनीतिक हित हैं। आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान पर निर्भर है। खाड़ी देशों को पाकिस्तान के कार्यबल और सैन्य संबंधों से लाभ होता है। रूस के दोनों देशों के साथ "गर्मजोशी भरे रिश्ते" और संयम बरतने का आह्वान उसके संतुलनकारी कार्य को दर्शाता है।
भारत-पाकिस्तान संघर्षों के लंबे इतिहास ने वैश्विक थकान को जन्म दिया है। कई राष्ट्र हिंसा के आवर्ती चक्र में उलझने से बचने के लिए तटस्थता को प्राथमिकता देते हैं।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर 70 देशों को जानकारी देने सहित भारत की सक्रिय कूटनीति आत्मविश्वास को प्रदर्शित करती है, लेकिन इसे आक्रामक माना जा सकता है। कुछ लोगों का सुझाव है कि वैश्विक राजनीतिक गतिशीलता को गलत तरीके से समझने और अमेरिकी मध्यस्थता पर निर्भरता ने इसकी क्षेत्रीय स्थिति को कमजोर किया है।
भारत की विदेश नीति का पुनर्मूल्यांकन
ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की विदेश नीति की ताकत और कमजोरियों दोनों को उजागर किया है। इस ऑपरेशन ने दिखाया कि भारत की सेना आधुनिक है और उन्नत, संपर्क रहित हमले करने में सक्षम है। लेकिन इसने कुछ गंभीर कूटनीतिक चुनौतियों को भी उजागर किया।
भारत के पड़ोसी देशों, जैसे बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका ने ऑपरेशन का खुलकर समर्थन नहीं किया। इससे पता चलता है कि "पड़ोसी पहले" की नीति ने संकट के समय में मजबूत क्षेत्रीय एकता का निर्माण नहीं किया है। भारत अब क्षेत्र में पाकिस्तान के प्रभाव को कम करने के लिए इन देशों के साथ अपने आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकता है।
भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से मिलकर बने क्वाड ने ऑपरेशन सिंदूर पर कोई टिप्पणी नहीं की। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि समूह भारत-पाकिस्तान तनाव पर नहीं, बल्कि चीन पर अधिक केंद्रित है। भारत को क्वाड से अपनी अपेक्षाओं पर पुनर्विचार करने और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों से निपटने के लिए शंघाई सहयोग संगठन जैसे अन्य मंचों पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।
भारत ने अपने हमलों को मापा हुआ और गैर-बढ़ावा देने वाला बताया, जिसे इज़राइल और पनामा जैसे देशों से समर्थन मिला। लेकिन कुछ वैश्विक प्रतिक्रियाएँ कम सकारात्मक थीं। यूरोपीय संघ ने भारत की आलोचना की और तुर्की ने पाकिस्तान का पक्ष लिया। इससे पता चलता है कि भारत को अपने कार्यों को दुनिया के सामने पेश करने के तरीके में सुधार करने और नागरिकों को नुकसान पहुँचाने के पाकिस्तान के दावों का प्रभावी ढंग से जवाब देने की आवश्यकता है।
भारत को अब वैश्विक समर्थन, विशेष रूप से इस्लामी देशों और ग्लोबल साउथ के देशों से समर्थन प्राप्त करते हुए आतंकवाद पर अपने सख्त रुख पर कायम रहने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसे पिछले अभियानों से मिले सबक पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। 2016 के उरी सर्जिकल स्ट्राइक भी सटीक थे, लेकिन इसने वैश्विक चिंता कम की। ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि भारत ने कूटनीतिक रूप से तैयारी की थी। सिंदूर की तरह, 2019 के बालाकोट एयरस्ट्राइक ने पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया। बढ़ने की आशंकाओं के कारण वैश्विक प्रतिक्रिया भी सीमित थी। लेकिन भारत ने मजबूत कूटनीति के माध्यम से इसके बाद की स्थिति को संभाला। इससे पता चलता है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर पर वैश्विक प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए बालाकोट से सीख सकता है। अधिकांश देशों की तटस्थ प्रतिक्रिया से पता चलता है कि भारत को लचीला और स्वतंत्र बने रहने के लिए अपने कूटनीतिक प्रयासों को व्यापक बनाना चाहिए।
भारत की कूटनीति की विफलता, भारत ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सैन्य हमला, भारत पाकिस्तान संघर्ष, वैश्विक प्रतिक्रिया ऑपरेशन सिंदूर, भारत की कूटनीति की विफलता, भारत की विदेश नीति 2025, ऑपरेशन सिंदूर की व्याख्या, जैश-ए-मोहम्मद का हमला, लश्कर-ए-तैयबा के शिविर, भारत पाकिस्तान तनाव, क्वाड प्रतिक्रिया भारत, यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया सिंदूर, अमेरिकी प्रतिक्रिया ऑपरेशन सिंदूर, भारत पर अरब देशों का हमला, भारत की सैन्य सफलता, भारत का वैश्विक अलगाव, भारत ने पीओजेके पर हमला किया, अजीत डोभाल की कूटनीति, भारत बनाम पाकिस्तान 2025, भारतीय वायु सेना का ऑपरेशन, भारत की वैश्विक छवि, भारत की रक्षा नीति, दक्षिण एशिया में आतंकवाद, भू-राजनीति भारत 2025, भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंध, भारत के पड़ोसियों की चुप्पी, भारत का वैश्विक समर्थन, रणनीतिक कूटनीति भारत