भारत में जाति व्यवस्था एक गहरी जड़ जमाए बैठी सामाजिक संरचना है, जिसने सदियों से देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया है। जाति जनगणना, जिसमें जनसांख्यिकीय डेटा के साथ-साथ जाति पहचान की व्यवस्थित गणना शामिल है, विभिन्न जाति समूहों के वितरण और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को समझने का एक साधन है। जबकि जाति जनगणना की मांग भारतीय राजनीति में एक आवर्ती विषय रही है, राष्ट्रीय जनगणना में इसका समावेश विवादास्पद रहा है। हाल ही में, राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेताओं द्वारा लगातार वकालत के बाद, आगामी दशकीय जनगणना में जाति जनगणना को मंजूरी देने के मोदी सरकार के फैसले ने इसके निहितार्थों के बारे में बहस को फिर से हवा दे दी है। यह निबंध भारत में जाति जनगणना के इतिहास, इसकी मांग की उत्पत्ति और मोदी सरकार द्वारा हाल ही में इस मांग को स्वीकार करने के पीछे की राजनीतिक मंशा का पता लगाता है।
1. भारत में जाति जनगणना का इतिहास
औपनिवेशिक शासन के तहत शुरुआती शुरुआत
भारत में जातियों की गणना करने की प्रथा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान शुरू हुई थी। पहली व्यवस्थित जाति जनगणना 1881 में भारत की दशकीय जनगणना के हिस्से के रूप में आयोजित की गई थी, जिसकी शुरुआत 1871-72 में हुई थी। ब्रिटिश प्रशासन ने इन जनगणनाओं का उपयोग जाति, धर्म और व्यवसाय के आधार पर जनसंख्या को वर्गीकृत करने के लिए किया, जिसका उद्देश्य विविध भारतीय समाज को अधिक प्रभावी ढंग से समझना और उस पर शासन करना था। 1901 तक, जनगणना ने 1,646 अलग-अलग जातियों की पहचान की, जो 1931 तक बढ़कर 4,147 हो गई, जो भारत के सामाजिक ताने-बाने की जटिलता को दर्शाती है। 1931 की जनगणना अंतिम व्यापक जाति-आधारित जनगणना बनी हुई है, जिसमें विस्तृत डेटा प्रदान किया गया है जो बाद में मंडल आयोग की सिफारिशों जैसी नीतियों को सूचित करता है। हालाँकि, 1941 की जनगणना ने जाति के आंकड़े एकत्र किए लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रसद संबंधी बाधाओं का हवाला देते हुए इसे प्रकाशित नहीं किया।
स्वतंत्रता के बाद बदलाव
1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार ने अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को छोड़कर राष्ट्रीय जनगणना में जाति गणना को बंद करने का फैसला किया। 1951 की जनगणना से लागू किया गया यह निर्णय जातिविहीन समाज के नेहरूवादी दृष्टिकोण पर आधारित था, जिसका उद्देश्य सामाजिक विभाजन को मजबूत करने से बचना था। सरकार का मानना था कि जाति पर ध्यान केंद्रित करने से भेदभाव को बढ़ावा मिल सकता है और राष्ट्रीय एकता में बाधा आ सकती है। इसके बजाय, राज्यों को 1961 से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की अपनी सूचियाँ संकलित करने की अनुमति दी गई, जिससे खंडित और असंगत डेटा सामने आए।
2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी)
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के कार्यकाल के दौरान जाति डेटा की मांग फिर से प्रमुखता से उठी। 2010 में, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), समाजवादी पार्टी (एसपी) और जनता दल (यूनाइटेड) जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के दबाव के कारण 2011 की जनगणना के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) की घोषणा की गई। लगभग ₹4,900 करोड़ की लागत से आयोजित, SECC 1931 के बाद से देश भर में जाति डेटा एकत्र करने का पहला प्रयास था। हालाँकि, इसे 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत आयोजित नहीं किया गया था, जिससे डेटा प्रकटीकरण स्वैच्छिक हो गया और महत्वपूर्ण त्रुटियाँ हुईं - जाति विवरण में 81,958,314 त्रुटियाँ, जिनमें से 14,577,195 को 2015 तक ठीक नहीं किया गया। जाति डेटा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सौंप दिया गया था, लेकिन सटीकता और संभावित सामाजिक ध्रुवीकरण पर चिंताओं के कारण यह अप्रकाशित है।
राज्य स्तरीय पहल
राष्ट्रीय जाति डेटा की अनुपस्थिति में, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों ने अपने स्वयं के जाति सर्वेक्षण किए। बिहार के 2023 के जाति सर्वेक्षण, एक ऐतिहासिक पहल, ने खुलासा किया कि ओबीसी और अत्यंत पिछड़े वर्ग (ईबीसी) राज्य की आबादी का 63% से अधिक हिस्सा हैं, जिससे देश भर में जनगणना की माँग बढ़ गई। इन राज्य-स्तरीय प्रयासों ने सकारात्मक कार्रवाई और कल्याण नीतियों को सूचित करने के लिए सटीक जाति डेटा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
2. जाति जनगणना की मांग की उत्पत्ति
प्रारंभिक मांगें और मंडल आयोग
ऐतिहासिक रूप से जाति जनगणना की मांग हाशिए पर पड़े समुदायों, विशेष रूप से ओबीसी से आई है, जिन्होंने सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को सही ठहराने के लिए सटीक डेटा की मांग की थी। 1979 में स्थापित और 1980 में रिपोर्ट करने वाले मंडल आयोग ने 1931 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ओबीसी आबादी का अनुमान 52% लगाया था। सरकारी नौकरियों और शिक्षा में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की इसकी सिफारिश ने जाति के आंकड़ों को राजनीतिक रूप से तीव्र ध्यान में ला दिया। हालाँकि, अद्यतन जाति के आंकड़ों की कमी ने कार्यान्वयन को विवादास्पद बना दिया, जिससे नई जनगणना की माँग बढ़ गई।
राजनीतिक दल और सामाजिक न्याय
स्वतंत्रता के बाद के भारत में जाति जनगणना की पहली महत्वपूर्ण राजनीतिक मांग 1990 के दशक के अंत में उभरी। 1998 में, संयुक्त मोर्चा सरकार ने 2001 की जनगणना में जाति को शामिल करने के लिए एक कैबिनेट नोट तैयार किया, लेकिन बाद की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिसमें गृह मंत्री एल.के. आडवाणी ने संभावित सामाजिक विभाजन का हवाला दिया। 2010 में इस मुद्दे ने फिर से जोर पकड़ा, जब यूपीए-2 के कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से 2011 की जनगणना में जाति को शामिल करने का आग्रह किया, जिसके परिणामस्वरूप SECC की शुरुआत हुई। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और एम. करुणानिधि जैसे क्षेत्रीय नेता इसके मुखर समर्थक थे, उनका तर्क था कि समान संसाधन आवंटन और प्रतिनिधित्व के लिए जाति डेटा आवश्यक था।
राहुल गांधी की वकालत
कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा (2022-2023) के बाद से जाति जनगणना के लिए एक प्रमुख आवाज़ रहे हैं। उन्होंने लगातार तर्क दिया है कि हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व और अधिकार सुनिश्चित करने के लिए जाति जनगणना आवश्यक है, जिसे “जितनी आबादी, उतना हक” (जनसंख्या के हिस्से के अनुपात में अधिकार) के नारे में समाहित किया गया है। गांधी ने सरकारी पदों पर ओबीसी, एससी और एसटी के कम प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाला है, उन्होंने कहा कि भारत सरकार में केवल 7% सचिव इन समूहों से आते हैं। उन्होंने आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने और निजी शैक्षणिक संस्थानों को कोटा बढ़ाने का भी संकल्प लिया है, जाति जनगणना को प्रणालीगत सुधार के लिए एक उपकरण के रूप में तैयार किया है।
मांग के लिए तर्क
जाति जनगणना की मांग कई कारकों से प्रेरित है:
नीति निर्माण: लक्षित कल्याण योजनाओं और सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को डिजाइन करने के लिए सटीक जाति डेटा महत्वपूर्ण है। इसके बिना, सरकारें पुराने या अधूरे अनुमानों पर निर्भर करती हैं, जिससे असमान संसाधन वितरण होता है।
कानूनी अनिवार्यता: सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण नीतियों को बनाए रखने के लिए जाति-वार डेटा की आवश्यकता पर बार-बार जोर दिया है, जैसा कि स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाले मामलों में देखा गया है।
सामाजिक न्याय: जाति जनगणना सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को उजागर कर सकती है, जिससे हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के लिए नीतियाँ बनाई जा सकती हैं। यह समानता और सामाजिक न्याय के लिए संवैधानिक जनादेश के अनुरूप है।
राजनीतिक रणनीति: विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस के नेतृत्व वाले भारत ब्लॉक के लिए, जाति जनगणना भाजपा के हिंदुत्व के आख्यान का जवाब है, जो सामाजिक न्याय के बैनर तले ओबीसी और दलित मतदाताओं को एकजुट करती है।
3. मोदी सरकार द्वारा जाति जनगणना की मांग को स्वीकार करना
निर्णय और इसका समय
30 अप्रैल, 2025 को, मोदी सरकार ने घोषणा की कि आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जाति गणना शामिल होगी, जो 2021 में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा व्यक्त किए गए अपने पहले के रुख को पलट देती है, जिन्होंने कहा था कि सरकार एससी और एसटी के अलावा अन्य जातियों की गणना नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCPA) द्वारा स्वीकृत यह निर्णय अक्टूबर-नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनावों से पहले आया है और 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में भाजपा की चुनावी हार के बाद आया है, जहाँ उसे 80 में से केवल 33 सीटें मिलीं।
राजनीतिक प्रेरणाएँ
मोदी सरकार द्वारा जाति जनगणना की माँग को स्वीकार करना राजनीतिक मजबूरियों और रणनीतिक गणनाओं के मिश्रण से प्रेरित है:
विपक्षी कथन का मुकाबला: विपक्ष, विशेष रूप से राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक ने 2024 के लोकसभा चुनावों में जाति जनगणना को एक केंद्रीय मुद्दा बनाया, इसे सामाजिक न्याय के एक उपकरण के रूप में पेश किया। भाजपा, जो शुरू में इस मांग की आलोचना करती थी, को नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और लोक जनशक्ति पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों जैसे सहयोगियों से दबाव का सामना करना पड़ा, जो जनगणना का समर्थन करते हैं। इसे मंजूरी देकर, भाजपा का उद्देश्य विपक्ष के चुनावी मुद्दे को बेअसर करना और ऐतिहासिक निर्णय का श्रेय लेना है।
ओबीसी समर्थन को मजबूत करना: भाजपा ने जाति-आधारित राजनीति का मुकाबला करने के लिए ऐतिहासिक रूप से ओबीसी सहित व्यापक हिंदू मतदाता आधार पर भरोसा किया है। हालांकि, जातिगत रेखाओं को धुंधला करने का प्रयास करने वाले इसके हिंदुत्व एजेंडे को बढ़ती जाति चेतना से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां ओबीसी मतदाताओं का 50% से अधिक हिस्सा हैं। जाति जनगणना भाजपा को प्रतिनिधित्व की उनकी मांगों को संबोधित करके ओबीसी से अपील करने की अनुमति देती है, खासकर उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनावी हार के बाद।
बिहार का चुनावी संदर्भ: बिहार, जहां 2023 के जाति सर्वेक्षण ने एक मिसाल कायम की है, राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण राज्य है। भाजपा के सहयोगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति जनगणना का समर्थन किया है, और इसकी राष्ट्रीय स्वीकृति राज्य चुनावों से पहले उनकी स्थिति को मजबूत करती है। भाजपा की स्थानीय इकाई ने भी बिहार सर्वेक्षण का समर्थन किया, जो क्षेत्रीय राजनीतिक गतिशीलता को दर्शाता है।
आरएसएस का समर्थन: सितंबर 2024 में, भाजपा के वैचारिक अभिभावक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए जाति जनगणना का समर्थन किया, बशर्ते इसका इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए न किया जाए। अपने पहले के विरोध से यह बदलाव भाजपा के फैसले के लिए वैचारिक कवर प्रदान करता है।
कानूनी चुनौतियों का सामना करना: आरक्षण नीतियों के लिए जाति-वार डेटा पर न्यायपालिका के जोर, राज्य-स्तरीय सर्वेक्षणों के साथ, राष्ट्रीय जनगणना के लिए दबाव बना है। मोदी सरकार का कदम अदालती हस्तक्षेप से बचने के लिए कानूनी और प्रशासनिक अनिवार्यताओं के अनुरूप है। राजनीतिक निहितार्थ
जाति जनगणना के दूरगामी निहितार्थ हैं:
सकारात्मक कार्रवाई: डेटा 50% आरक्षण सीमा को संशोधित करने, ओबीसी कोटा को उप-वर्गीकृत करने और निजी संस्थानों में आरक्षण बढ़ाने की मांग को जन्म दे सकता है, जैसा कि राहुल गांधी ने वकालत की है।
चुनावी राजनीति: जनगणना राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्रों को नया रूप दे सकती है और परिसीमन अभ्यास को प्रभावित कर सकती है, खासकर विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण को जनगणना के आंकड़ों से जोड़कर। यह जाति-आधारित लामबंदी को भी तेज कर सकता है, जो भाजपा की एकीकृत हिंदू पहचान की कहानी को चुनौती दे सकता है।
सामाजिक गतिशीलता: जबकि समर्थकों का तर्क है कि जाति जनगणना असमानताओं को दूर करेगी, आलोचकों को डर है कि यह जाति की पहचान को मजबूत कर सकती है और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दे सकती है। सरकार ने इन चिंताओं को कम करने के लिए एक “पारदर्शी” प्रक्रिया पर जोर दिया है।
अभी क्यों?
मोदी सरकार का निर्णय राजनीतिक वास्तविकताओं के प्रति व्यावहारिक प्रतिक्रिया को दर्शाता है। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के निरंतर अभियान ने जाति जनगणना को एक शक्तिशाली मुद्दा बना दिया है, खासकर ओबीसी और दलित मतदाताओं के बीच। भाजपा की चुनावी असफलताओं, सहयोगियों के दबाव और आरएसएस के नरम रुख के कारण, इस दिशा में सुधार की आवश्यकता है। जनगणना को मंजूरी देकर, भाजपा का लक्ष्य सामाजिक न्याय की कहानी को पुनः प्राप्त करना, बिहार में अपने गठबंधन को मजबूत करना और महत्वपूर्ण चुनावों से पहले विपक्ष की आलोचना को रोकना है। हालांकि, स्पष्ट समयसीमा की कमी कार्यान्वयन के बारे में सवाल उठाती है, विपक्षी नेता ठोस तारीखों की मांग कर रहे हैं।
निष्कर्ष
भारत में जाति जनगणना एक जटिल मुद्दा है जिसकी गहरी ऐतिहासिक जड़ें और महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव हैं। औपनिवेशिक जनगणना में इसकी उत्पत्ति से लेकर स्वतंत्रता के बाद इसके बंद होने तक, जाति की गणना सामाजिक न्याय और विभाजन पर बहस से भरी रही है। जाति जनगणना की मांग, जो शुरू में क्षेत्रीय नेताओं द्वारा संचालित और बाद में राहुल गांधी द्वारा समर्थित थी, प्रणालीगत असमानताओं को संबोधित करने के लिए डेटा की आवश्यकता को दर्शाती है। मोदी सरकार की हाल ही में 30 अप्रैल, 2025 को घोषित की गई मंजूरी, विपक्षी कथाओं का मुकाबला करने, ओबीसी समर्थन को मजबूत करने और बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में चुनावी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक रणनीतिक कदम है। जबकि जनगणना सकारात्मक कार्रवाई और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को नया आकार देने का वादा करती है, इसकी सफलता पारदर्शी कार्यान्वयन और सामाजिक नतीजों के सावधानीपूर्वक प्रबंधन पर निर्भर करती है। जैसा कि भारत अपने जाति प्रश्न से जूझ रहा है, जाति जनगणना एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बनी हुई है, बशर्ते इसका उपयोग विभाजन के बजाय उत्थान के लिए किया जाए।
जाति जनगणना, जाति जनगणना भारत, भारत जाति जनगणना 2025, जाति जनगणना समझाया, ओबीसी आरक्षण, मंडल आयोग, भारतीय राजनीति 2025, जाति व्यवस्था भारत, बिहार जाति सर्वेक्षण, राहुल गांधी जाति जनगणना, ओबीसी डेटा भारत, एससी एसटी ओबीसी आरक्षण, 2025 चुनाव भारत, भारतीय राजनीतिक विश्लेषण, मोदी सरकार जाति जनगणना, सामाजिक न्याय भारत, सकारात्मक कार्रवाई भारत, भारत जाति सर्वेक्षण, जाति राजनीति भारत, जाति आधारित आरक्षण
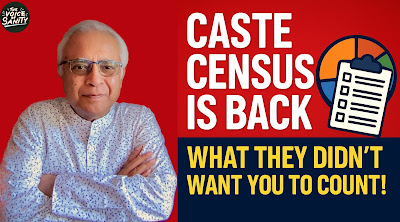



No comments:
Post a Comment